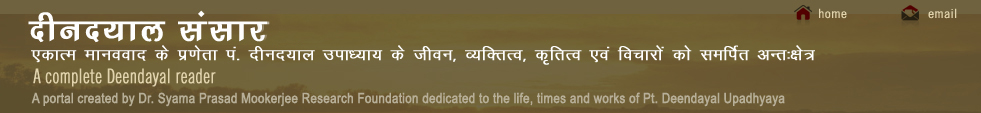Lecture - 1st, on April 22nd 1965 Lecture - 2nd, on April 23rd 1965 Lecture - 3rd, on April 24th 1965 Lecture - 4th, on April 25th 1965 Presidential Speech at Calicut in Kerala in
December 1967
अध्याय-1, 25 अप्रैल, 1965
कल हमने राष्ट्र के अंतर्गत राज्य के कार्यों पर विचार विमर्श किया था। भारतीय परम्परा के अनुसार एक राष्ट्र उन लोगों की बदौलत होता है जो उसमें रहते हैं और उसका सृजन किसी समूह के द्वारा नहीं किया जाता और जबर्दस्ती उसे बनाया भी नहीं जा सकता । राष्ट्र की आवश्यकतानुसार कई प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं जो उसे मौलिक व्यवस्था प्रदान करती हैं। राज्य इन संस्थाओं में से ही एक है और नि:संदेह उसकी अहम् भूमिका है लेकिन वह सर्वोपरि नहीं है। हमारे साहित्य में जहाँ-राजा के कर्तव्यों का वर्णन है, उसके महत्व के दिग्दर्शन होते हैं। संभवतया इसीलिए उसके उत्तारदायित्वों का भी उल्लेख किया जाता है ताकि उसे इसका एहसास हो। अपनी प्रजा के जीवन एवम् चरित्र पर राजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अत: उसे अपने व्यवहार में बेहद कुशलता का निर्वाह करना पड़ता है। महाभारत में भीष्म यही कहते हैं जब उनसे राजा के कर्तव्यों के बारे में पूछा जाता है कि क्या परिस्थितियों के वशीभूत राजा बनता है अथवा राजा परिस्थितियों का सृजन करता है? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परिस्थितियों को आकार देने में राजा की ही भूमिका होती है। इस तथ्य का अर्थ कई लोग इस तरह लगाते हैं कि राजा सबसे बड़ा है और सर्वोपरि है जो कि सत्य नहीं है। भीष्म ने यह नहीं कहा कि राजा धर्म से भी परे है। यह कथन सत्य है कि राष्ट्रीय विकास और समृध्दि में राजा की अहम भूमिका होती है लेकिन सही मायने में वह तो धर्म का ही रक्षक है। उसे केवल यही देखना है कि उसकी प्रजा धर्म के अनुरूप जीवन यापन कर रही है या नहीं लेकिन राजा यह निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है कि धर्म में उसकी इच्छा को भी शामिल किया जाए। आज के इस युग में राजा की अहमियत आज की कार्यकारिणी की तरह ही है।
आज के संदर्भ में राज्य के अंतर्गत कानूनों के विधिवत रूप से निष्पादन का दायित्व कार्यकारिणी का है लेकिन कानून बनाने का उसका अधिकार नहीं है। जब कार्यकारिणी ईमानदारी और दक्षतापूर्ण ढंग से कार्य नहीं करती तो नियमों अर्थात कानून की धज्जियाँ उड़ जाती है। यह सब हम अपने चारों तरफ देखते आए हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि ''कार्यकारिणी ही आज के ताण्डव के लिए उत्तारदायी है।'' आखिर निषेधाज्ञा पर अमल क्यों नहीं होता? कौन इस कमी के लिए उत्तारदायी है? एक संस्था और एक निकाय को जब इसका दायित्व सौंप दिया गया है तो इसके असफल होने का क्या कारण है? क्यों इसका ठीक कार्यान्वयन नहीं होता? जब आप इतने गिर जाते हैं कि एक दलाल से भी मासिक लेने की सोचते हैं, तो कैसे इसका अनुपालन हो पाएगा? कार्यकारिणी ही वास्तव में इसके अनुपालन के लिए उत्तारदायी है। यही भीष्म का कथन था महाभारत में कि राजा के सर्वोपरि होने पर भी धर्म-विरुध्द कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि क्रूर राजा वेनु को हरा कर उसके स्थान पर पृथु को राजा क्यों बनवाते। इतिहास में ऋषियों के इस कार्य पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई वरन् इसके विपरीत इस कार्य की प्रशंसा की गई। जब धर्म के महत्व को सर्वोपरि रख कर कर्म किया जाता है तो ऋषि तो धर्म के ही संरक्षक थे जिनके कार्य को कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सका और राजा की गलतियों के लिए उसे हटा कर दूसरे धर्मात्मा व्यक्ति को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। अन्यथा राजा को हराना अवैध होता और ऋषियों के कार्यक्षेत्र का विषय नहीं माना जाता। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि धर्म की राह पर कभी न चलने वाले राजा को उसकी गद्दी से हटाना सभी के दायित्व के अन्तर्गत आता है। पाश्चात्य देशों में किसी राजा को या तो किसी दूसरे राजा ने हटाया अथवा जनता ने राजा की सार्वभौमिक सत्ताा छीन ली। वहाँ राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता रहा और परिस्थितियों और सिध्दान्तों के आधार पर उसे नहीं हटाया जा सका।
हमारे सामाजिक-राजनैतिक स्थापना में राजा और राज्य कभी भी सर्वोपरि नहीं माने गए। इतना ही नहीं कई और भी संस्थाएं (राज्य के अतिरिक्त, जो उनमें से एक थी) रहीं जिनकी स्थापना सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए की गई। ये संस्थाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन की सहभागी रहीं। हमने पंचायतें और जनपद संभाएँ विकसित कीं। राजा ने सर्वाधिकार-सम्पन्न होते हुए भी इनका कभी विरोध नहीं किया। व्यापार के आधार पर भी ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इनकी भी राज्य ने कभी अनदेखी नहीं की और उनकी व्यवस्था को मान्यता दी जाती रही। अपने-अपने क्षेत्रों के सफल संचालन के लिए उन्होंने अपने नियम तथा विनियम बनाए। विभिन्न समुदायों की पंचायतों, जनपद सभाओं और ऐसे अन्य संगठनों ने अपनी नियमावली बनाई। राज्य का कार्य यह देखना था कि इन नियमों को संबंधित व्यक्तियों ने देख लिया है जिन पर इन्हें लागू होना है। राज्य ने कभी भी इन नियमों में दखल नहीं दिया उसका कार्य तो समाज की सुव्यवस्था के विशेष पहलुओं पर ही केन्द्रित था।
इसी तरह कुछ आर्थिक क्षेत्रों में कई संस्थाएं सृजित की गईं। हमारे आर्थिक ढाँचे की क्या प्रकृति अथवा व्यवस्था हो, हमें इसे देखना लाज़मी है। हमारी आर्थिक व्यवस्था उस तरह की हो जिसमें हमारी संस्कृति, मानवीय गुण तथा राष्ट्रीय धरोहर पुष्पित एवं पल्लवित हो और उसमें निरंतर विकास होता रहे। हमें अपनी बुराईयाँ तथा कुरीतियाँ त्याग कर ऊँचाइयों पर पहुंचाना ही हमारी व्यवस्था का उद्देश्य है। हमारी धारणा है कि मानवीय गुणों के निरंतर विकास की प्रक्रिया से ही संपूर्णता और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यदि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारी आर्थिक प्रणाली का ढाँचा तथा विनियम कैसे होने चाहिएँ, अब जरा इस बात पर विचार करें।
देश के विकास और देशवासियों की दैनिक वस्तुओं की संपूर्ति के लिए और उत्पादन वृध्दि के लिए आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे हर स्थिति में पूरी करने का उद्देश्य लेकर इस व्यवस्था को नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए? मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति के उपरांत अधिक समृध्दि और विकास के लिए क्या और अधिक उत्पाद किया जाना चाहिए। यह प्रश्न बार-बार उठता है और हम पाते हैं कि पाश्चात्य समाज इस बात को काफी आवश्यक समझता है कि अधिक से अधिक इच्छाएं जीवन में हों और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सामान्यतया होता यही है कि इच्छा के अनुरूप ही व्यक्ति उत्पादन करता है। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। लोग अब उत्पादन के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं।
मांग के अनुरूप उसका उत्पादन करने के बजाए तो बाजार अनुसंधान के जरिए मांग के सृजन के लिए प्रयास किए जाते हैं। पहले उत्पादन माँग के अनुसार होता था जबकि आज माँग उत्पादन के अनुसार है। यही पाश्चात्य आर्थिक आंदोलन की प्रमुख पहचान है । चाय का ही हम उदाहरण लें। चाय का उत्पादन इसीलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं और उसे मांगते हैं। अब उसका उत्पादन वृहत स्तर पर है और लोगों के वह मुँह लग चुकी है और सामान्य उपयोग की वस्तु बन गई है। इतना ही नहीं आज वह हमारे जीवन का अंग बन गया है। इसी तरह वनस्पति घी का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि कोई भी इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहता था। पहले इसका उत्पादन हुआ फिर हमें बताया गया कि इसका प्रयोग करें। यदि उत्पादित माल का उपयोग नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से उसमें संकुचन हुआ।
1930-32 के वाकये को कौन नहीं जानता। जब माल था लेकिन उसकी मांग नहीं थी। अत: फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। दिवालियापन तथा बेरोजगारी चारों तरफ देखी गई। इस प्रकार अब यह अत्यंत आवश्यक है कि जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है उसका उपयोग किया जाए।
साप्ताहिक ''ऑर्गनाइजर'' के संपादक एक बार अमेरिका गए जहाँ से लौट कर उन्होंने एक मजेदार घटना सुनाई।
उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक कंपनी आलू छीलने का उत्पाद बनाती थी। उत्पादन काफी बढ़ने के बाद जब इसकी बिक्री कम होने लगी तो कंपनी ने इसके विक्रेताओं की बैठक बुलाई कि किस तरह इस उत्पाद की बिक्री बढ़ाई जाए ताकि सभी उपभोक्ता इसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित भी हों और विवश हों। एक सुझाव दिया गया कि इसकी पैकिंग बेहतर कर दी जाए ताकि लोग इसे नया समझ कर इसका प्रयोग करने लगे। एक सुझाव यह आया कि इसका रंग बिल्कुल आलू के छिलके की तरह कर दिया जाए ताकि आलू के छिलकों के साथ चाहे गलती से ही, लोग इसे कूड़े में डाल दें और नए की मांग करें। हालांकि यह कदम कोई अच्छा नहीं था लेकिन कंपनी ने ऐसा ही किया और उसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती गई और अधिशेष स्टॉक बिक गया। लोगों की आवश्यकताओं और मांग को संतुष्ट न कर नई मांग का सृजन करना आज के आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य बन गया है। पुराना फेंको नए खरीदो ही उनका आज का गणित है। माना कि हमें सीमित प्राकृतिक वस्तुओं की कोई चिंता नहीं है लेकिन प्राकृतिक संतुलन के लिए तो हमें चिन्ता करनी होगी। अत: बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण उत्पादों को बनाया जा रहा है ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सकें लेकिन दूसरी तरफ जो नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिससे सभ्यता और मानवता दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
अत: यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम उतना ही दोहन करें जिसके किए वह सक्षम हों। फलों की प्राप्ति के लिए पेड़ों को तहस-नहस नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन पर असर तो होगा ही। लेकिन अमेरिका में अधिक उत्पादन के लिए जिन रसायनों का प्रयोग वहाँ की जमीन पर हुआ था, वह आज उपज योग्य नहीं रही। लाखों एकड़ ऐसी भूमि आज अमेरिका में है जिस पर खेती नहीं हो सकती। यह विनाश कब तक चलेगा?
जब मशीनों का धीरे-धीरे मूल्यहा्रस हो जाता है और बाद में वे बेकार पड़ जाती है तो उन मशीनों को खरीदने के लिए मूल्यहा्रस के लिए हम कब फंड बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमें यह एहसास कर लेना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्रणाली को उपलब्ध संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए ताकि वह भविष्य के उपयोग के लिए वह बंजर न हो जाए। उद्देश्यपूर्ण जीवन, खुशहाली तथा प्रगति के लिए भौतिक उद्देश्यों पर सकारात्मक चिंतन आवश्यक है। प्रकृति ने मानव के लिए सब कुछ व्यवस्था की है लेकिन उपभोग और उत्पादन की अंधी दौड़ ने हमें इस तरह का बना दिया है कि हम सोचते हैं कि मानव उपभोग के लिए ही पैदा हुआ है। विधिवत कार्य करने के लिए इंजन को कोयले की आवश्यकता है लेकिन वह केवल कोयले के उपयोग के लिए ही नहीं बना है। हमें यह देखना होगा कि न्यूनतम कोयले के प्रयोग से अधिकतम उर्जा हम कैसे ले सकते हैं। आर्थ्ािक दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना चाहिए। मानव के बारे में भी हमें यही सोचना होगा कि न्यूनतम उपभोग से वह अधिकतम शक्ति कैसे प्राप्त करे। यही प्रणाली तो सभ्यता कहलाएगी जिसमें मानव के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि उसके परम लक्ष्य को हमें देखना होगा। इस प्रणाली से हम प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकतानुसार ही करेंगे जिसके साथ-साथ उसका पालन-पोषण भी हमारा दायित्व होगा। प्रकृति के साथ एक शिशु की तरह जीना हमारा उद्देश्य होना चाहिए न कि उसके दोहन में लीन होकर विनाश करना। तभी जाकर एक संतुलन स्थापित होगा और जीवन फलेगा-फूलेगा।
इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण आर्थिक प्रणाली को प्रेरित करता है जिससे हमारे चिंतन में आर्थिक प्रश्न नए रूप ले लेंगे। पश्चिमी अर्थशास्त्र में चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो अथवा सामाजिक मूल्य की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आर्थिक विषय वस्तु का केन्द्र बिन्दु मूल्य पर आधारित है। मूल्य का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है जो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सामाजिक दर्शनिक जो मूल्य पर ही आधारित है, इसे अपूर्ण, अमानवीय तथा कुछ हद तक तथ्यहीन मानते हैं। उदाहरण के लिए एक नारा जो हमेशा ही प्रयोग में लाया जाता रहा है, वह है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए रोटी कमाना है।'' सामान्यतया कम्यूनिस्ट इस नारे का प्रयोग करते हैं लेकिन पूंजीवादी भी इसे अस्वीकार नहीं करते। यदि उनके बीच में कोई मतभेद है, वह केवल इतना ही है कि कोई कितना कमाता है और कितना जमा करता है। पूंजीवादी यह मानते हैं कि पूंजी और उद्यम दोनों ही पूंजीगत व्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं और यदि ये लाभ के प्रमुख अंश प्राप्त करते हैं तो वे इसे इनकी योग्यता का मापदण्ड मानते हैं। दूसरी ओर कम्यूनिस्ट केवल श्रम को ही उत्पादन का प्रमुख उपादान मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी विचार उपयुक्त नहीं है। वास्तविक रूप से हमारा नारा यह होना चाहिए कि जो कमायेगा वह खिलाएगा और हर एक के पास खाने के लिए पर्याप्त होगा। भोजन की प्राप्ति तो जन्मसिध्द अधिकार है। कमाने की योग्यता शिक्षा और प्रशिक्षण है। समाज में जो कमाता नहीं है उसे भी भोजन का अधिकार है। बच्चे और बूढ़े, बीमार तथा अपाहिज सभी कमाते तो नहीं है लेकिन खाने के अधिकारी हैं। आर्थिक प्रणाली इस कार्य के लिए मुहैया करवाई जानी चाहिए। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस उत्तारदायित्व के लिए उत्तारदायी नहीं है। एक आदमी केवल रोटी के लिए ही नहीं कमाता, वह अपने उत्तारदायित्व के निर्वाह के लिए भी कमाता है। अन्यथा जिनके पास खाने की व्यवस्था है, वे काम क्यों करते?
किसी भी आर्थिक प्रणाली को व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की व्यवस्था करनी ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएँ हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। समाज के दायित्व को निर्वाह करने के लिए शिक्षा भी बेहद आवश्यक है। अंत में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके विधिवत इलाज तथा देखरेख का दायित्व समाज का है। यदि कोई सरकार इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करती है तो उसे हम धर्म का राज कहेंगे अन्यथा उसे अधर्म राज्य कहा जाएगा। राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कालीदास ने रघुवंश में कहा है कि वे ''अपनी प्रजाजनों की देखरेख एक पिता की तरह करते थे और उनकी रक्षा और शिक्षा के पूरे दायित्व का निर्वाह करते थे''। राजा भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था, वे भी अपनी प्रजा की ''देखरेख, लालन-पालन और उनकी रक्षा पिता की तरह करते थे''। यह उन्हीं का देश भारत है। यदि आज उनके इस देश में प्रजा की देखरेख और रक्षण जो प्रजाजनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है, नहीं किया जाता तो भारत का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
शिक्षा - एक सामाजिक उत्तारदायित्व
समाज के हित एवम् विकास के लिए बच्चों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जन्म से एक बच्चा जानवर के समान ही है। वह समाज का जिम्मेदार सदस्य केवल शिक्षा और संस्कृति के कारण ही बन पाता है। समाज के हित के लिए शुल्क लेने का प्रचलन हुआ। यदि शुल्क न दे पाने के कारण कोई अशिक्षित रह जाता है, तो समाज इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। हम पेड़ पौधों को लगाने और उसके संभरण के लिए कोई शुल्क नहीं देते। इसके विपरीत हम अपना धन और प्रयास इस व्यवस्था में लगाते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल लगेंगे। जिनका हम उपयोग करेंगे।
शिक्षा भी इसी तरह का निवेश है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करता है। दूसरी ओर इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर समाज से विमुख भी हो जाते हैं। 1947 से पूर्व सभी रियासतों में शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। उच्चतर शिक्षा गुरुकुलों में नि:शुल्क थी और यहाँ तक कि खाने और रहने की व्यवस्था भी वहाँ नि:शुल्क दी जाती थी। विद्यार्थी समाज में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते थे। कोई भी घर विद्यार्थियों को भिक्षा देने के लिए इंकार नहीं करता था। दूसरे शब्दों में समाज शिक्षा के बोझ को वहन करता था।
इसी तरह यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि चिकित्सा पर किए गए खर्च को देना पड़े। वास्तव में चिकित्सा उपचार भी नि:शुल्क होना चाहिए जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आज कल तो मंदिर में प्रवेश के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। तिरुपति में बालाजी मंदिर में प्रवेश शुल्क 0.25 पैसे देना पड़ता है। फिर भी दोपहर में एक घंटे के लिए कोई टिकट नहीं देना पड़ता जिसे धर्म दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुल्क देकर जाना मानो अधर्म दर्शन हो। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, देखरेख और प्रगति के दायित्व की समाज को गारंटी दी जानी चाहिए। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की संपूर्ति की गारंटी दी जाती है तो उसके लिए संसाधन कहाँ से आ पाएँगे?