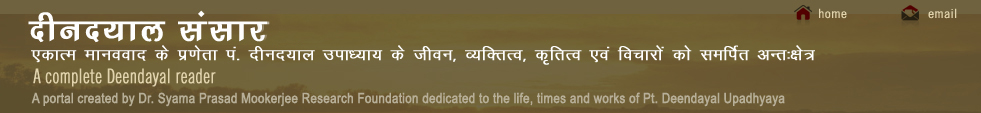Lecture - 1st, on April 22nd 1965 Lecture - 2nd, on April 23rd 1965 Lecture - 3rd, on April 24th 1965 Lecture - 4th, on April 25th 1965 Presidential Speech at Calicut in Kerala in
December 1967
अध्याय-1, 24 अप्रैल, 1965
कल हमने मानव के स्व-अस्तित्व पर विचार किया था। स्व-अस्तित्व या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू और व्यक्ति की आवश्यकताओं के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए और सभी स्तरों पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की परिपूर्णता के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है। परन्तु मानव की केवल व्यक्तिगत पहचान पर्याप्त नहीं है। शरीर, बुध्दि, तथा आत्मा केवल ''मैं'' के अन्तर्गत नहीं आता वरन् उसका अस्तित्व ''हमें'' में ही निहित है। अत: हमें समूह और समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। यह सत्य है कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है लेकिन समाज कैसे अस्तित्व में आया, इस संबंध में दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न मत हैं। पश्चिम से जुडे हुए लोगों पर जहाँ पश्चिमी-सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव है, उनका मानना है की ''समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसका अस्तित्व व्यक्तियों द्वारा मिलकर परस्पर समझौते, के लिए है। ''इस दृष्टिकोण को सामाजिक संपर्क सिध्दान्त का नाम दिया गया है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है। विभिन्न पाश्चात्य दृष्टिकोणों में अंतर इन प्रश्नों के कारण है कि ''यदि व्यक्ति समाज का सृजन करता है तो मुख्य संचालन शक्ति किसके हाथ में होगा? समाज के अथवा व्यक्ति के? क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समाज को बदल दे? क्या समाज अपने नियमों को व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करेगा और प्रत्येक से निष्ठा की अपेक्षा रखेगा अथवा व्यक्ति इन प्रश्नों को मानने के लिए स्वतंत्र है?''
व्यक्ति बनाम-समाज
इस प्रश्न पर पश्चिम में काफी विवाद है। कुछ लोगों का वहाँ यह मत रहा कि समाज के लिए वह सर्वोपरि है जिस कारण विवाद का जन्म हुआ। सत्य तो यह है कि यह दृष्टिकोण कि व्यक्ति से समाज का जन्म हुआ, मूल रूप से गलत है। यह सत्य है कि समाज का निर्माण कई व्यक्तियों के समूह से होता है लेकिन यह भी सत्य है कि समाज लोगों की मल्कियत है, न की कुछ व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से बना झुण्ड, हमारे मत से समाज स्वत: जन्म लेता है। एक व्यक्ति की ही तरह समाज का अस्तित्व भी कायम हुआ। लोगों ने समाज नहीं बनाए। समाज कोई क्लब नहीं अथवा कोई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी अथवा पंजीकृत सहकारी समिति नहीं है। वास्तव में समाज की अपनी अलग आत्मा है, उसका अपना जीवन है, यह व्यक्ति की तरह सार्वभौमिक है। हमने इस दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं किया कि समाज एक मध्यस्थ संस्था है। इसका अपना जीवन है। इसका अपना शरीर, मस्तिष्क, बुध्दि तथा आत्मा है। कुछ पश्चात्य मनोवैज्ञानिक इस सत्य को अब स्वीकार करने लगे हैं। मैकडुगल ने मनोविज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया जिसे ''ग्रुप माइंड'' की उन्होंने है संज्ञा दी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समूह का अपना मस्तिष्क, अपना अलग मनोविज्ञान तथा चिंतन और कार्य के इसके अपने तरीके हैं। समूह की भावनाएं भी हैं। ये भावनाएं व्यक्तिगत भावना के पूर्ण रूप से समान नहीं है। सामूहिक भावनाएं व्यक्तिगत भावना का गणितीय रूप से योग करने का नाम नहीं है, न ही सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्तियों का योगदान है। समूह की शक्ति, बुध्दि, भावनाएं व्यक्तिगत भावना से एकदम अलग हैं। अत: कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कमजोर होने पर भी एक व्यक्ति समाज का नायक बन जाता है। कई बार एक व्यक्ति अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन समाज की बेइज्जती उसके बर्दाश्त के बाहर होती है। हो सकता है एक आदमी अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती को बर्दाश्त कर जाए अथवा भूल जाए लेकिन वह आदमी समाज को भला-बुरा कहने वाले को क्षमा न कर पाए। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत चरित्र काफी ऊंचा हो लेकिन समाज के सदस्य के रूप में वह बेकार हो। इसी तरह एक व्यक्ति समाज में अच्छा हो सकता है लेकिन हो सकता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में वह उतना अच्छा न हो। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
इस तथ्य को एक उदाहरण से स्पष्ट करें, एक बार श्री विनोबा जी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी की इस प्रश्न पर वार्ता चल रही थी कि हिंन्दुओं और मुसलमानों के चिंतन में अंतर कहाँ पाया जाता है। गुरुजी ने विनोबा जी को बताया की हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हिंदुओं में ईमानदार और अच्छे लोग ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है और ऐसी ही स्थिति मुसलमानों की भी है। इसी तरह राक्षसी वृति के लोग भी दोनों ही समाजो में है। किसी भी समाज में अच्छे लोगों का एकाधिकार नहीं है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हिंदुओं में जो व्यक्तिगत तौर पर राक्षसी वृति के हैं जब समाज में साथ मिल कर कार्य करते हैं तो हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। दूसरी ओर जहाँ दो मुसलमान साथ हो जाते हैं, वे ऐसी बातें सोचते हैं जो वे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोच पाते। वे अलग तरह से सोचना शुरू कर देते है। यह नित प्रति दिन का हमारा अनुभव है। विनोबा जी ने स्वीकार किया की इस बात में सत्यता है लेकिन उस पर आगे चर्चा नहीं की।
यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं की व्यक्ति और समाज के चिंतन का दायरा अलग-अलग है। इन दोनों में गणितीय संबंध नहीं है। यदि एक हजार अच्छे लोग परस्पर एकजुट हो जाएं तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता की वे उसी तरह से अच्छी बातों को सोचेंगे जैसाकि वे व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं।
यदि हम बीस साल पूर्व के भारतीय विद्यार्थियों की तुलना आज के विद्यार्थियों से करें तो हम पाते हैं की आज का औसत विद्यार्थी पहले की तुलना में कमजोर और सहमा हुआ है। हर तरह से वह कमजोर और सहमा हुआ है लेकिन जब ऐसे विद्यार्थी एक समूह में आ जाते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। तब ये हर तरह उत्तारदायित्व-विहीन कार्य कर बैठते हैं। इस प्रकार एक विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत तौर पर अनुशासित लगता है लेकिन ऐसे ही विद्यार्थियों का समूह अनुशासन से मुँह मोड़ कर गलत कार्य कर बैठते हैं। हमें विचार करना होगा की ऐसा परिवर्तन होता क्यों है। इसे ''झुण्ड की मानसिकता'' कहेंगे जो व्यक्तिगत मानसिकता से अलग होती है। झुण्ड की मानसिकता में मस्तिष्क पूरी तरह जागृत नहीं रहता, जब व्यक्तियों का एक समूह कुछ समय के लिए एकत्रित हो जाता है तो ऐसे झुण्ड को ''झुण्ड मानसिकता'' वाले लोगों का समूह कहा जाएगा, परंतु समाज में सामाजिक मानसिकता काफी लंबे अंतराल के बाद विकसित होती है। जब व्यक्तियों का समूह दीर्घकाल के लिए परस्पर एक हो जाता हैं तो ऐतिहासिक परम्पराएं एवम् सहयोग एक आचरण की तरह बन जाता है और लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं उनके रिवाज़ एक जैसे बन जाते हैं। यह सत्य है कि साथ रहने से एक-रूपता स्थापित होती है। एकसी सोच वाले दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री स्वाभाविक हो जाती है। फिर भी एक तरह के आचार-व्यवहार से कोई समाज अथवा राष्ट्र प्रगतिशील नहीं बन जाता।
शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए?
हम जानते हैं की कई पुरातन राष्ट्र मिट गए। पुरातन ग्रीक राष्ट्र का अंत हुआ। ईजिप्ट की सभ्यता भी मटियामेट हो गई। बेबिलोनिया तथा सीरिया की सभ्यताएं इतिहास का विषय बन कर ही रह गईं। क्या वहाँ कभी ऐसा समय था जब लोगों ने साथ रहना छोड़ दिया? तथ्य तो यह है कि लोगों के बीच गहरे अंतर आए जिस कारण इन राष्ट्रा का पतन हो गया। ग्रीस ने एलेक्जैंड़र तथा हेरेडोट्स जैसे शासक दिए। उलाइसिस, अरस्तू, सुकरात तथा प्लेटो जैसे दर्शनिकों का देश आज भी उन्हीं की विरासत हैं। उनके अनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि ग्रीस में पूरी जनसंख्या अपनी संस्कृति से अलग-थलग हो गई। पिता और पुत्र की संस्कृति वहाँ हमेशा जीवंत रही। यह संभव है कि पुरातन 250 से लेकर 500 पीढ़ियों पुराना ग्रीस आज भी वहाँ विघमान है वह कैसे समाप्त हो सकता है। पुरानी सभ्यता वहाँ आज भी देखने को मिलती है। पुराना ग्रीस, और पुराना ईजिप्ट आज नहीं रहे और उनके स्थान पर नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ऐसा कैसे हुआ, यह प्रश्न विचारणीय है। यह सामान्य तथा विवाद-रहित है कि राष्ट्रों का अस्तित्व केवल साथ में रहने से नहीं होता। इज्राइल के यहूदी सदियों से तमाम इधर-उधर से आए। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय भावना का स्रोत किसी स्थान विशेष में रहने के कारण नहीं है वरन् यह कुछ और ही है। दरअसल राष्ट्रीय भावना समाज की सुदृढ़ता के लिए मूलमंत्र की तरह है जिसमें रच बस कर वह सम्प्रदाय फल फूल सकता है।
राष्ट्र क्या है ?
जनता के सामने लक्ष्य का स्रोत राष्ट्र ही है। जब जनसमूह एक लक्ष्य और एक आदर्श के सामने नतमस्तक हो जाता है और एक विशेष भू-भाग की मातृभूमि मानने लगता है तो ऐसे समूह को हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। शरीर में एक ''आत्मा'' है जो किसी भी व्यक्ति की चिति शक्ति की तरह है। यह शक्ति ही उसकी प्राणशक्ति है जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह माना जाता है कि मानव बार-बार जन्म लेता है लेकिन दूसरे जन्म में वह दूसरा ही व्यक्ति कहलाएगा और अलग ही व्यक्ति माना जाएगा। वही आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो पहले से विभिन्न व्यक्तित्व की जन्मदात्री बन जाती है। आदमी की मृत्यु कुछ नहीं वरन् शरीर से आत्मा का बहिर्गमन मात्र ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति में काफी परिवर्तन होते हैं। जीव वैज्ञानिक हमें बताते है कि इस दौरान व्यक्ति में अनन्त परिवर्तन होते हैं। चूंकि शरीर में आत्मा का निवास होता है, अत: शरीर तब तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें आत्मा अथवा प्राणशक्ति है। शरीर और आत्मा का संबंध एक नाई के उस्तरे की तरह का हैं।
शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए?
एक बार एक ग्राहक की दाढ़ी बनाते हुए नाई ने ग्राहक को अपना उस्तरा दिखाते हुए कहा कि यह 60 वर्ष पुराना उस्तरा है। मेरे पिता भी इसी उस्तरे से अपने ग्राहकों की दाढ़ी बनाते थे। ग्राहक काफी आश्यर्च चकित था क्योंकि उस्तरे का हैंडल काफी चमकदार था और लगता था जैसे कि नया हो। आचर्श्च चकित ग्राहक बोला कि ''यह हैंडल इतना चमकदार कैसे है?'' आपने इन 60 सालों में इसकी चमक को कैसे बरकरार रखा। नाई ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस हैंडल को 60 वर्षों तक चमकदार रखना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हमने 6 महीने पहले ही इसे बदलवाया था, बड़ी सहजता से उसने जवाब दिया। ग्राहक ने फिर उत्सुकतावश प्रश्न किया कि स्टील कितना पुराना है? उत्तर में वह बोला कि स्टील तीन वर्ष पुराना है। वास्तव में हैंडल बदल दिया गया था, स्टील बदल दिया गया था लेकिन रेजर (उस्तरा) पुराना ही रहा और उसकी पहचान बनी रही। इसी तरह एक राष्ट्र की अपनी आत्मा है। जन संघ ने अपनी नीतियों में इसे ''चिति'' का नाम दिया। अर्थात राष्ट्र की चिति शक्ति ही उसकी आत्मा का स्वरूप है। मैकडुगल के अनुसार यह शक्ति ही अंतरंग प्रकृति की शक्ति है। व्यक्तियों का हर समूह इसी प्रकृति की इसी शक्ति से प्रभावित और प्रवाहित होता है। इसी तरह हर समाज की अंतरंग शक्ति अजन्मा होती है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं होती।
एक मानव का जन्म आत्मा के साथ होता है जो उसकी प्राण शक्ति भी है। आत्मा और चरित्र अलग अलग हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गतिशील संगठन है और एक व्यक्ति के चिंतन और उसके प्रभाव का चित्रांकन है। लेकिन आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं है। उसी तरह राष्ट्रीय चरित्र निरंतर बदलता रहता है और ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों के वशीभूत होता है। संस्कृति संस्थाओं, प्रयासों एवं समाज के इतिहास से बनती है और पनपती है जिसका समावेश राष्ट्रीय चरित्र में होता ही होता है। लेकिन इन सभी बातों का समावेश ''चिति'' में नहीं होता। ''चिति'' तो सार्वभौम है जो राष्ट्र की अंतरंग शक्ति है। ''चिति'' किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान की पथ प्रदर्शक होती है। चिति के अनुरूप ही संस्कृति का उत्थान होता है।
चिति, संस्कृति एवम् धर्म
इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत की कहानी के वृतान्त को लेते हैं। महाभारत के युध्द में कौरवों की हानि हुई जबकि पांडव विजयी हुए। हम धर्म के सम्बन्ध में पांडवों के चरित्र को उदात्ता क्यों मानते हैं? यह युध्द राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया गया वरन् धर्म के लिए किया गया। युधिाष्ठिर की प्रशंसा और दुर्योधन की निन्दा राजनैतिक कारणों के लिए नहीं की जाती जिसके लिए कृष्ण ने कंस का वध किया था। इसके लिए हम कृष्ण को अवतार मानते हैं और कंस को असुर की संज्ञा दी जाती है।
Top