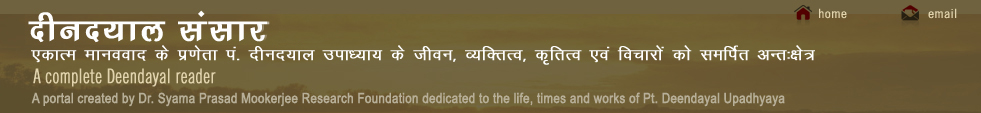‘सब को काम’ ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार
(पांचजन्य, 31 अगस्त, 1953)
बेकारी की समस्या यद्यपि आज अपनी भीषणता के कारण अभिशाप बनकर हमारे सम्मुख खड़ी है किंतु उसका मूल हमारी आज की समाज, अर्थ और नीति व्यवस्था में छिपा हुआ है। वास्तव में जो पैदा हुआ है तथा जिसे प्रकृति ने अशक्त नहीं कर दिया है, काम पाने का अधिकारी है। हमारे उपनिषद्कार ने जब यह घोषणा की कि 'काम करते' हुए हम सौ वर्ष जीएँ (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समा:।) तो वे यही धारणा लेकर चले कि प्रत्येक को काम मिलेगा इसीलिए शास्त्रकारों ने प्रत्येक के लिए कर्म की व्यवस्था की। यहाँ तक कि इस आशंका से कि कोई कर्महीन रहकर केवल भोग की ही ओर प्रवृत्त न हो जाए उन्होंने यह धारणा प्रचलित की कि यह भारतभूमि 'कर्मभूमि' है। स्वर्ग के देवता भी अपने कर्म फल क्षय हो जाने पर यही इच्छा करते हैं कि वे भारत में जन्म लें एवं पुन: सुकृत संचय करें। तात्पर्य यह कि हमने किसी भी व्यक्ति के संबंध में बेकारी अथवा कर्म विहीनता की कल्पना नहीं की। अत: भारतीय अर्थनीति का आधार 'सबको काम' ही हो सकता है। बेकारी अभारतीय है। भारतीय शासन का कर्तव्य है कि वह इस आधार को लेकर चले।
बेकारी के कारण
लोगों को काम न मिलने के दो ही कारण हैं। प्रथम, तो काम के लिए जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हो, वैसी योग्यता उनमें न हो। दूसरे, काम करनेवालों का इतना बाहूल्य हो कि उद्योग धंधे, व्यापार एवं सार्वजनिक सेवाओं का वर्तमान स्तर उन्हें खपा न पाएँ। बेकारी के अन्य कारण भी हैं किंतु वे तात्कालिक एवं अस्थायी हैं। भारत में आज दोनों ही कारण उपस्थित हैं। अत: बेकारी के प्रश्न को हल करने के लिए हमें इनके संबंध में गंभीरता से विचार करना होगा। शिक्षा की पद्धति और उद्योग धंधों के विकास के संबंध में अपनी नीति निश्चित करनी होगी। इस नीति के साथ बेकारी को दूर करने का प्रश्न ही नहीं, देश की समृद्धि का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।
अर्थ-नीति का आधार
भारत की जनसंख्या, उसके सात लाख गाँव, उसका विस्तार, भारतीय जन की प्रकृति, हमारी समाज-व्यवस्था, युगों से चली आई हमारी अर्थ-नीति की परंपरा आदि का विचार कर आज सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि भारतीय समृद्धि का आधार हमारे कुटीर एवं ग्रामोद्योग ही हो सकते हैं। हाँ, यूरोपीय अथवा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कुछ अपवादस्वरूप व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो इन उद्योगों में मध्ययुगीन संस्कृति की बू पाते हैं तथा जो इन्हें अप्रगतिशील मानकर इंग्लैंड और अमेरिकी पद्धति पर बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने की सलाह देते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि किसी भी दिशा में अतरेककर अंतिम कोटि का विचार प्रस्तुत करना बुद्धिमानी नहीं होगी। फिर भी हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था का कोई केंद्र अवश्य निश्चित कर लेना होगा जिसके चारों ओर एवं जिसके हित-संवर्धन में बड़े पैमाने पर उद्योगों को हम अपना केंद्र बनाएँ? आज इस दृष्टि से हमारी स्थिति बहुत ही गिरी हुई है। दूसरे देशों के मुकाबले में बड़े उद्योगों में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यदि उस दृष्टि से हम कुछ करना चाहें तो हमें मशीन और तंत्र-विशारदों के लिए ही नहीं बल्कि पूँजी के लिए भी दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ेगा। पिछले छह वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं और अपना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा चुके हैं। हमें जन-शक्ति की दृष्टि से भी विचारना होगा। इन बड़े कारखानों में यदि हजारों को काम मिलता है तो दूसरी ओर लाखों बेकार हो जाते हैं।
यदि कल्पना कर भी ली जाए कि संपूर्ण भारत में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण होने पर चारों ओर सुख और समृद्धि लौटने लगेगी किंतु जब तक हम अपने को पूरी तरह उजाड़ चुके होंगे। इस परिवर्तन में करोड़ों नष्ट हो जाएँगे तथा संभव है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही जन-क्षोभ की ज्वाला में भस्म हो जाएँ। अत: हमारा केंद्र तो होना चाहिए मनुष्य। मनुष्य को काम मिले और वह सुखी रहे यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मशीन मनुष्य की सुविधा के लिए है, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। मनुष्य मशीन का निर्माता है, उसका स्वामी है, उसका गुलाम नहीं। उत्पादन के साधन की दृष्टि से उसका उपयोग अवश्य है किंतु वह मनुष्य को खाकर नहीं उसे खिलाकर होना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य श्रम और मशीन में एक समन्वय चाहिए जो प्रत्येक समाज धीरे-धीरे करता जाता है। ज्यों-ज्यों उद्योगों की अवस्था में उन्नति होती जाती है, उनको बाजार मिलता जाता है, मनुष्य स्वयं मशीनों का सहारा लेता है। किंतु जब यही अस्वाभाविक रूप से किया जाता है तो हानि होती है। अत: भारत में कुटीर और ग्रामोद्योग ही हमारे केंद्र हो सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योग इन उद्योगों के हित में जहाँ चलाना आवश्यक हो चलाए जाएँ किंतु इनके प्रति स्वार्थी बनकर नहीं।
औद्योगीकरण कैसे?
आवश्यकता है कि वेग के साथ औद्योगीकरण का कार्यक्रम अपनाया जाए। इसके लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को आधार बनाकर, बड़े उद्योगों को उनके साथ समन्वित किया जाए। वे एक-दूसरे के प्रति स्पर्धी न बने इसका ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से कुछ सुझाव नीचे दिए जाते हैं
- केंद्र में एवं प्रांतों में उन उद्योगों के रक्षण एवं विकास के लिए आयोगों की स्थापना हो।
- छोटे उद्योगों को कच्चा माल दिलाने की पूर्ण व्यवस्था की जाए। सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके अथवा पुरानी आढ़त की पद्धति का प्रचार करके यह व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अपनी ओर से गोदाम खोल सकती है।
- कारीगरों को कम दर पर कर्जा मिलने की व्यवस्था हो।
- छोटी मशीनें जो विद्युत् से भी चल सकें उन्हें उपलब्ध कराई जाएँ तथा उन्हें विद्युत् शक्ति देने का प्रबंध हो।
- मशीन और कच्चा माल अगाऊ मिल सके तथा उसका भुगतान तैयार माल से अथवा किश्तों में हो।
- तैयार माल की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो। सहकारी संस्थाओं के द्वारा अथवा सहकारी क्रय भंडारों द्वारा यह व्यवस्था हो। सरकार इस बात का दायित्व ले कि वह कारीगरों द्वारा तैयार माल को, यदि वह बाजार में नहीं बिकता, तो उचित मूल्य पर खरीद लेगी।
- स्थान-स्थान पर इन उद्योगों की दृष्टि से अनुसंधान केंद्र खोले जाएँ।
- रेल भाड़े की दरों में कुटीर उद्योगों के माल के अनुरूप परिवर्तन किया जाए।
- बड़े कारखाने केवल उन वस्तुओं के खोले जाएँ जिनका विकेंद्रीकरण संभव न हो, इनके उत्पादन की सीमाएँ एवं क्षेत्र, निश्चित कर दिए जाएँ।
- विदेशी माल पर नियंत्रण कर स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाए।
- सरकारें अपनी आवश्यकता की पूर्ति कुटीर उद्योगों के माल से ही करें।
- कारीगरों को शिक्षा देने के लिए उद्योग शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए।
- कुटीर उद्योगों के माल को बिक्री कर आदि करों से मुक्त कर दिया जाए।
- दूतावासों में केवल स्वदेशी तथा विशेषत: कुटीर उद्योग निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग हो।
बेकारी को रोकने एवं उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वसाधारण की क्रयशक्ति बढ़नी चाहिए। इसके लिए आय की विषमता दूर कर उसमें समानता स्थापित करनी होगी। शासन की कर-नीति इस लक्ष्य की प्राप्ति में दूर तक नहीं ले जाती। निम्न और मध्यवर्ग के लोगों को कर मुक्त कर ऊपर के वर्ग पर कर का भार बढ़ाना होगा। बड़े-बड़े लोग पूँजी के दब जाने का शोर मचाकर भार से बचते रहते हैं किंतु यह ठीक नहीं। यदि आर्थिक विषमता बनी रही तथा नीचे के लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी तो पूँजी निकालकर भी कोई लाभ नहीं। वास्तव में तो जो चीज पैदा होती है उसके खरीददार मिलते गए तो उद्योग पनपता जाएगा। अत: पैदा किए हुए माल के लिए माँग पैदा करना उद्योगों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस माँग की कमी के कारण ही बेकारी पैदा होती है।
औद्योगिक शिक्षा
अक्षर और साहित्य ज्ञान के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाए। औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि विचार बहुत दिनों से हो रहा है किंतु अभी तक सिवाय कुछ औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के खोलने के साधारण शिक्षा का मेल औद्योगिक शिक्षा से नहीं बैठाया गया है। टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें। वे भी नौकरी की ही तलाश में घूमते हैं। कारण, जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अयोग्य बना देती है। अत: आवश्यक तो यह होगा कि गाँवों के धंधे, खेती और व्यापार के साथ हमें शिक्षा का मेल बैठाना होगा। प्रथमत: शिक्षा की प्रारंभिक एवं माध्यमिक अवस्थाओं में हमें विद्यार्थी को उसके घरेलू धंधे के वातावरण से अलग करने की जरूरत नहीं। बल्कि हम ऐसा प्रबंध करें कि वह उस वातावरण में अधिक-से-अधिक रह सके तथा अज्ञात रूप से वह धंधा सीख सके। धीरे-धीरे हमें यह भी प्रयत्न करना होगा कि वह अपने अभिभावकों का सहयोगी बन सके। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने तक नवयुवक को अपना धंधा भी आ जाना चाहिए। हो सकता है कि उन धंधों की योग्यता के प्रणामपत्र की भी हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़े। माध्यमिक शिक्षा तक कुशाग्र बुद्धि सिद्ध होनेवाले नवयुवकों की आगे शिक्षा का प्रबंध उनकी रुचि के अनुसार किया जाए।
जनसंख्या उसकी आवश्यकता में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन एवं व्यवस्था, इन तीनों का पारस्परिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तब अर्थ-संबंधी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। आज देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है किंतु उसके अनुपात में उत्पादन के साधन और उत्पादन नहीं बढ़ रहा। फलत: हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पातीं। अत: हमारा रहन-सहन स्तर बहुत ही नीचा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम उत्पादन के साधनों की वृद्धि के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें। इसके लिए हमारी निगाह स्वाभाविक ही पश्चिम के बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा उत्पादन की ओर चली जाती है और हम पिछले छह वर्षों से उसके लिए प्रत्यनशील हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या उन साधनों से हम देश के सभी लोगों को काम दे सकेंगे यदि नहीं तो उन साधनों के स्वामी एवं उनपर काम करनेवाला एक छोटा सा वर्ग रह जाएगा। फलत: उत्पादित वस्तुओं का समान रूप से वितरण नहीं होगा। बचे हुए लोगों को या तो जनसेवा के रूप में लगाना होगा अथवा हमारी आवश्यकताएँ इतनी विभिन्न प्रकार की हो जाएँ जिससे उसकी पूर्ति के लिए सबको खपा सकें तथा उनके साधन जुटा सकें। यह भी संभव है कि हम कानून बनाकर जहाँ चार लोगों से काम चल जाएँ वहाँ दस लोगों को रखने की सलाह दें यह प्रजातांत्रिक देश में व्यापक रूप से संभव नहीं है। आज बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के साधन जुटाना भी हमारे लिए कठिन हो रहा है तथा उस प्रतिक्रिया में हम छोटे उद्योगों के साधनों को भी नष्ट कर रहे हैं। अब बेकारी प्रमुखतया यांत्रिक है। यंत्र मनुष्य की जगह लेता जा रहा है तथा मनुष्य बेकार होता जा रहा है। यंत्र का अर्थ प्रगति समझा जाता है और इसलिए हमारी प्रगतिवादी मनोवृत्ति यंत्रीकरण से विमुख नहीं होने देती। हमें इस संबंध में समन्वयात्मक दृष्टि से काम करना होगा। हमारी नीति का आधार होना चाहिए प्रत्येक को काम।
प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे काम मिले। काम न मिलने से उसकी व्यक्तिगत आजीविका का सहारा तो जाता ही रहता है, वह राष्ट्र की संपत्ति के अर्जर में सहायता देने से भी वंचित हो जाता है। प्रत्येक को काम का सिद्धांत यदि स्वीकार कर लिया तो 'समवितरण' की दिशा में निश्चित हो जाती है। अधिक केंद्रीकरण के स्थान पर हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते जाते हैं।
ज X क X य = इ
प्रत्येक को काम का सिद्धांत स्वीकार करने पर बाकी बातों का भी निर्धारण हो सकता है। गणित के छोटे से सूत्र के रूप में हम अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत रख सकते हैं
ज X क X य = इ
यहाँ 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा का द्योतक है जिसकी पूर्ति की उसमें शक्ति है।
'ज' समाज के काम करने योग्य व्यक्तियों का द्योतक है।
'क' काम करने की अवस्था एवं व्यवस्था का द्योतक है।
'य' यंत्र का द्योतक है।
इस सूत्र के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि 'ज' निश्चित रहे तो 'इ' के अनुपात में 'क' और 'य' को बदलना होगा। ज्यों-ज्यों हमारी माँग बढ़ती जाएगी हमें ऐसे यंत्रों का उपयोग करना होगा जिनके सहारे हम अधिक उत्पादन कर सकें। आज शासन जिस नीति पर चल रहा है उसमें 'य' सबका नियंत्रण कर रहा है।
वास्तव में तो 'इ' प्रभावी माँग के बढ़ने से ही हमारी समस्या हल होगी किंतु 'इ' सहज ही नहीं बढ़ सकती क्योंकि यह हमारी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। अत: शासन को देश की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न भी करना होगा।
'इ' अर्थात् प्रभावी माँग देश में तथा देश के बाहर भी हो सकती है। यदि हमारा माल बाहर जाता है तो 'इ' बढ़ जाती है। बाहर से माल आने पर देशज वस्तुओं की दृष्टि से 'इ' कम हो जाती है क्योंकि हमारी कार्य-शक्ति का बहुत बड़ा भाग बाहर से आई वस्तुओं की खरीद पर खर्च हो जाता है। आज यही हो रहा है। सरकार की आयात-नीति के कारण हमारे बाजार विदेशी माल से पट गए हैं। उनके सस्ते और अच्छे होने तथा 'स्वदेशी' प्रेम के अभाव के कारण उनकी भारी खपत है। फलत: स्वदेशी वस्तुओं के लिए 'इ' दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। चूँकि 'य' और 'क' में एकाएक परिवर्तन करना संभव नहीं इसलिए 'ज' कम होता जा रहा है। बेकारी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए जहाँ एक ओर विदेशी आयात की उन वस्तुओं पर जो स्वदेशी तैयार माल पर अनुचित रूप से दबाव डाल रही हों प्रतिबंध लगाना होगा तो हमारी ओर समाज में 'स्वदेशी' की भावना को भी जाग्रत करना होगा। विदेशी आयात पर नियंत्रण आयात-निर्यात एवं तटकर नीति के द्वारा किया जा सकता है। बड़े-बड़े उद्योगों को संरक्षण देने की नीति तो शासन में अंग्रेजी काल से ही अपनाई है। घरेलू ग्रामोद्योगों की ओर इस दृष्टि से कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें संरक्षण की नितांत आवश्यकता है और वह हमें देना ही होगा।
'इ' को बढ़ाने की दृष्टि से विदेशी व्यापार की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारी बहुत सी चीजों की विदेशों में खपत है। लड़ाई के जमाने में कपड़ा एवं कई अन्य वस्तुओं के लिए हमने मध्यपूर्व एवं सुदूरपूर्व के देशों में अपने बाजार बना लिए थे। काम की वस्तुओं के लिए तो आज भी अमेरिका और यूरोप के देशों में हमारे माल की काफी पूछ होती है। यदि प्रयत्न किया जाए तो ये बाजार भी बढ़ सकते हैं। फर्रुखाबाद की छींट और बनारस के रेशम के रुमालों की अमेरिका में बहुत भारी माँग है। किंतु सरकारी नियंत्रण नीति के कारण यह माँग ठीक तरह से पूरी नहीं हो पाई जबकि हम डालर कमाने के लिए बड़े उत्सुक रहे।
'ज' अर्थात् देश की जनसंख्या तो हमारे देश में बराबर बढ़ती जा रही है। उसे सहसा रोका नहीं जा सकता। अत: 'इ' की वृद्धि के अनुपात में हमको 'क' और 'य' पर नियंत्रण करना होगा। आज देश में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक तो आधुनिक यंत्रीकरण के बिलकुल विरोधी है तथा उसे कतई नहीं चाहते। दूसरे वे हैं जो अनियंत्रित रूप से यंत्रीकरण की वृद्धि चाहते हैं। हम समझते हैं दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। जैसाकि ऊपर के सूत्र से ज्ञात होगा 'य' ध्रुव नहीं, बल्कि 'इ' तथा अन्य तत्त्वों पर अवलिंबत है। यदि हमारी 'इ' हमारी बढ़ गई कि बिना यंत्रों की वृद्धि के हम उसे पूरा नहीं कर सकते तो हमें यंत्रीकरण करना ही होगा किंतु यदि माँग के बढ़े बिना हमने यंत्रीकरण करना स्वीकार कर लिया तो फिर 'ज' या 'क' में कमी करनी होगी। चूँकि 'क' को कम करना उत्पादन व्यय, समाज नीति आदि अनेक बातों पर निर्भर है, 'ज' कम हो जाएगा। अत: हमारा सिद्धांत है कि ज्यों-ज्यों देश की क्रय शक्ति एवं प्रभाव माँग बढ़ती जाए हम यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करते जाएँ। इस पद्धति में हमारा स्वाभाविक विकास होगा तथा हो सकता है कि हम अपनी स्थिति के अनुकूल अधिक उपयोगी यंत्रों का आविष्कार और निर्माण भी कर सकें।
क्या किया जाए?
बेकारी के इन कारणों को दूर करके समस्या को मौलिक रूप से हल करने के साथ ही आज जो बेकार हो गए हैं अथवा हो रहे हैं उनको फिर से काम देने की तथा जब तक काम नहीं मिलता तब तक उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। आज के बेकारों में बहुत बड़ी संख्या पढ़े-लिखे लोगों की है। उनको खपाने के लिए स्कूल खोलने की नीति सरकार ने अपनाई है। इस नीति को और भी व्यापक करना होगा।
स्कूल और कॉलेजों में तुरंत ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध कर देना चाहिए। जो 'अंतिम परीक्षा' पास करके निकलनेवाले हैं उनके लिए एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। इससे पढ़े-लिखे बेकारों की समस्या के हल की दौड़ में एक वर्ष तुरंत आगे बढ़ जाएँगे तथा संभव है कि एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में से बहुत से लोग बाबूगिरी की और न दौड़कर हाथ से रोजी कमाना शुरू कर दें।
युद्धकाल में कारखानेदारों को भारी मुनाफा हुआ था जो आजकल संभव नहीं है। अत: आज गिरे हुए मुनाफों को हानि की आशंका से चारों ओर बचन की योजनाएँ प्रारंभ हो गई है जिसका परिणाम मजदूरों पर भी पड़ता है। उनकी छटनी की जा रही है। सरकार भी अपने विभिन्न विभागों में छटनी कर रही है। कई विभागों का जैसे रसद और पूर्ति विभाग तथा युद्धकालीन अनेक विभागों का काम अब समाप्त हो गया है। उनके कर्मचारियों की भी छटनी अनिवार्य सी प्रतीत होती है। ये बेकारी समस्या को और भी भीषण बनाए हुए हैं। आवश्यकता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जब तक कहीं दूसरी नौकरी न मिल जाए उनकी जीविका की व्यवस्था की जाए। यूरोप के कई देशों में बेकारी बीमा योजना चालू है। अनैच्छिक रूप से बेकार होनेवाले श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है। भारत सरकार के श्रममंत्री श्री गिरि ने एक त्रिदलीयमिल मालिक, श्रमिक और शासन के बीच समझौता कराता है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के अनिच्छा से काम से अलग होने पर उसे पैंतालीस दिन तक अपने वेतन एवं महँगाई भत्ता का आधा मिलता रहेगा। इस संबंध में एक विधान भी लोकसभा में प्रस्तुत होने की आशा है। यह पग ठीक दिशा में उठाया गया है। किंतु मालिकों के ऊपर यह भार न छोड़कर शासन को इसकी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए तथा मालिकों से इस बीमा योजना में चंदा लेना चाहिए। साथ ही पैंतालीस दिन की अवधि न रखकर यह अवधि जब तक दूसरी नौकरी न मिले तब तक की रखनी चाहिए।
पढ़े-लिखे तथा लोगों की शिक्षा के औद्योगिक शिक्षा केंद्र खोले जाएँ जहाँ वे शिक्षा के साथ-साथ काम भी कर सकें। ये केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर खोले जाने चाहिए।
गाँवों की बेकारी को दूर करने के लिए सहायता कार्य प्रारंभ किए जाएँ। सड़के, इमारतें, बाँध, कुएँ और तालाब आदि की बहुत सी योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी जो योजनाएँ हैं उनमें जन-शक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अभी तो वहाँ भी श्रम बचानेवाली बड़ी-बड़ी मशीनों का ही उपयोग किया गया है।
अर्थ-नीति के निर्धारण में शासन का प्रमुख हाथ होने के कारण उसकी नीति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी और क्षमता बहुत अंशों में उसकी होती है। फिर भी जनता और राजनीतिक पार्टियाँ उस दृष्टि से अपने सीमित क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं। शासन को समस्या की गंभीरता का अनुभव कराने के लिए वे आंदोलन तो कर ही सकती हैं किंतु अपनी ओर से रचनात्मक सहयोग भी दे सकती है।
अपने क्षेत्र के छोटे-छोटे उद्योगों की तालिका बनाकर उनमें शिक्षार्थी के रूप में एक-एक, दो-दो व्यक्तियों को रखा जा सकता है। आज बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनमें रोजी कमाई जा सकती है। हाँ सीखे हुए लोगों की कमी है।
छोटे-छोटे उद्योग केंद्र भी सहकारी आधार पर चलाए जा सकते हैं। स्वदेशी की भावना एवं पारस्परिक संबंधों के सहारे उनके लिए बाजार भी मिल सकता है। इनके अतिरिक्त और भी रचनात्मक कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं।